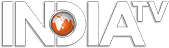31 अक्टूबर
1947 में देश का विभाजन हुआ था। एक से दो देश बन गए, लोग बंट गए, लोग कट भी गए। तब से लेकर अब तक इस त्रासदी पर कई फिल्में बन चुकी हैं और बन रही हैं। दरअसल ये वो नासूर है जो सदियों से रिसता रहा है। ऐसी ही एक त्रासदी 1984 में हुई थी जिसे सिख विरोधी दंगे कहा जाता है। ऑपेशन ब्लूस्टार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने ही गोली मार दी थी। शाम होते-होते पूरी दिल्ली में सिख विरोधी दंगा फैल गया था। घरों-गलियों में सिखों को मारा गया था। अंगरक्षकों के अपराध का बदला पूरे समुदाय से लिया जा रहा था। इस दंगे में सत्ताधारी पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। 32 साल हो चुके हैं उस ख़ून-ख़राबे को। इस बीच कई जांच आयोग बैठाए गए, उनकी रिपोटों भी आई लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 31 अक्टूबर के अगले कुछ दिनों तक चले इस दंगे में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2186 सिखों की जानें गई थीं। ग़ैरसरकारी आंकड़ा 9000 से ज़्यादा का है।
31 अक्टूबर’ फिल्म उसी खौफनाक रात की कहानी है। एक मध्यवर्गीय परिवार के किरदारों को लेकर हैरी सचदेवा ने इसका निर्माण किया है। फिल्म के निर्देशक शिवाजी लोटन पाटिल हैं। कम बजट वाली इस फिल्म में लेखक-निर्देशक के नेक इरादों के बावजूद उस रात के ख़ौफ़ की झलक भर दिखती है। लेखक-निर्देशक ने बहुत ही सतही तरीके से इसे पेश किया है। कथानक में गहराई और नाटकीयता नहीं है। इस विषय पर बनी फिल्म के लिए ज़रुरी नज़र लेखन, निर्देशन और दृश्य संयोजन में नहीं दिखाई देती। हो सकता है कि सीमित बजट इसकी एक वजह हो।
इस तरह के विषय पर फ़िल्म बनाना आसान नहीं होता क्योंकि इसके लिए न सिर्फ गहन रिसर्च की ज़रुरत होती है बल्कि बजट भी होना चाहिये। गांधी फिल्म के निर्देशक एटनबरो ने फिल्म बनाने के पहले 20 साल रिसर्च किया था। ’31 अक्टूबर’ इस फ़र्क को साफ़ दिखलाती है। बेशक़ फिल्म का सरोकार मानवीय और बड़ा है, प्रासंगिक भी है। हम आज भी देख सकते हैं कि कैसे उन्मादी समूह किसी एक धार्मिक समुदाय के ख़िलाफ़ होकर समाज में तबाही ला सकता है। ऐसे माहौल में पुलिस और प्रशासन दंगाइयों के साथ हो जाएं तो भयंकर तबाही हो सकती है। सिख विरोधी दंगों के साक्ष्य और रिपोर्ट इसके गवाह हैं। ’31 अक्टूबर’ मे देवेन्दर के परिवार के जरिए हम सिर्फ एक घर, एक परिवार और एक गली से गुजरते हैं। यानी ये फिल्म इतनी बड़ी त्रासदी का एक गलियारा मात्र है।
खौफ और अविश्वास के उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे, जो दोस्ती और मानवीयता के लिए जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटे। फिल्म उन्हें भी लेकर चलती है, लेकिन सद्भाव का प्रभाव स्थापित नहीं कर पाती। तकनीकी रूप से यह कमज़ोर फिल्म है। छायांकन से लेकर अन्य तकनीकी मामलों की कमियां फिल्म को बेअसर करती हैं। ‘31 अक्टूबर’ उस भयावह रात की यादें ताजा करती है, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश की काली गाथा बनी। अगर यह फिल्म भाईचारे और सद्भाव के संदेश को प्रभावशाली तरीके से कहानी में पिरोती तो आज की पीढ़ी के लिए सबक हो सकती थी। इस इरादे और उद्देश्य में यह फिल्म असफल रहती है।
सोहा अली खान और वीर दास ने मेहनत की है, लेकिन वे स्क्रिप्ट की सीमाओं में ही रह जाते हैं। सहयोगी किरदारों में आए कलाकार प्रभावहीन हैं।